Indian cinema and the need for remakes in the changing times
बदलते दौर में ‘भारतीय’ सिनेमा और रीमेक की ज़रूरत
एक समय था जब ‘साउथ की फ़िल्म’ कहने पर रजनीकान्त की एक्शन फ़िल्में दिमाग में आती थीं जिनमें भौतिकी के नियम उस तरह काम नहीं करते थे जैसे असल ज़िंदगी में करते हैं। ऐसा शायद इसलिए भी था कि हम तक इसी तरह की फ़िल्में ज़्यादा पहुँचती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर काफ़ी बदली है। साल 2015 में आई तेलुगु फ़िल्म ‘बाहुबली’ ने जब पूरे देश में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया तो एक क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्म के इस तरह ब्लॉकबस्टर होने पर हर कोई हैरान था। कुछ ही सालों बाद, आज हालत यह हो चुकी है कि हिंदी के दर्शक को दक्षिण की फ़िल्मों का भी उतना ही इंतज़ार रहने लगा है जितना कि हिंदी फ़िल्मों का। आज किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्म का दायरा न सिर्फ़ पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो सकता है। अब कई दक्षिण भारतीय फ़िल्मों को ‘पैन इंडिया’ और ‘वर्ल्डवाइड’ रिलीज़ मिल रही है। माना जाने लगा है कि किसी फ़िल्म को क्षेत्रीय स्तर पर रिलीज़ करके अलग-अलग भाषाओं में उसके रीमेक बनाने से अच्छा है कि उसी फ़िल्म को कई भाषाओं में डब करके पूरे देश में एक साथ रिलीज़ कर दिया जाए। दक्षिण के फ़िल्म निर्माता जहाँ कई तरह का मौलिक कंटेंट लेकर आ रहे हैं, बॉलीवुड के सामने ‘रीमेक इंडस्ट्री’ के लेबल से मुक्त होने की चुनौती है।
रीमेक का सिलसिला
दक्षिण से बॉलीवुड और बॉलीवुड से दक्षिण में रीमेक का लंबा इतिहास रहा है। हॉलीवुड की रीमेक तो हमारे यहाँ होती ही रहीं। इंटरनेट पर दक्षिण भारतीय फ़िल्मों की लम्बी फ़ेहरिस्त देखी जा सकती है जो बॉलीवुड फ़िल्मों की रीमेक थीं। ‘बावर्ची’, ‘यादों की बारात’, ‘दीवार’, से लेकर ‘3 ईडियट्स’, ‘अ वेडनेसडे’, ‘दबंग’, ‘अंधाधुन’ जैसी कई फ़िल्मों के दक्षिण में रीमेक हुए और उनमें से कई ने अच्छी कमाई भी की। अमिताभ की कई फ़िल्मों के रीमेक में रजनीकान्त ने काम किया। इसी दौरान हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी दक्षिण की फ़िल्मों के रीमेक होते रहे। मज़े की बात है कि दिलीप कुमार अभिनीत फ़िल्म ‘राम और श्याम’ एनटी रामाराव अभिनीत तेलुगु फ़िल्म ‘रामुडु भीमुडु’ का रीमेक थी। बाद में हिंदी में इसी विषय को लेकर हेमा मालिनी अभिनीत ‘सीता और गीता’ बनी जिसका रीमेक फिर से दक्षिण में जाकर तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में हुआ। जेमिनी स्टूडियोज़ जैसी निर्माण संस्थाओं और टी. रामाराव जैसे निर्देशकों ने दक्षिण भारतीय भाषाओं में फ़िल्में बनाकर खुद ही उनके हिंदी रीमेक भी किए। एक ही भाषा में फ़िल्मों के रीमेक हर जगह होते रहे हैं। एक ही उपन्यास पर कई बार फ़िल्में बनती रही हैं। यह विदेशों में भी होता आया है और हमारे यहाँ भी, जैसे ‘देवदास’ उपन्यास पर हिंदी में तीन बार फ़िल्में बनीं। लेकिन अलग-अलग कालखंड में फ़िल्म बनाने से निर्देशक के पास तकनीक और सिनेमैटोग्राफ़ी के ज़रिए कुछ नया करने की गुंजाइश होती है। रीमेक का यह सिलसिला आज भी जारी है लेकिन हालात अब काफ़ी बदल चुके हैं।
मल्टीप्लेक्स और टेलीविजन
इक्कीसवीं सदी शुरू होते-होते जब बॉलीवुड का सिनेमा सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स की तरफ़ खिसकने लगा था, ज़्यादातर फ़िल्में मल्टीप्लेक्स के दर्शक को ध्यान में रखते हुए बनाई जाने लगीं। इन फ़िल्मों के नायक-नायिकाएँ ‘मेट्रोसेक्शुअल’ होने लगे और कंटेंट में एक खास तरह की विविधता आने लगी। इससे फ़िल्मकारों को मसाला फ़िल्मों से अलग कुछ नया करने का मौका मिला, साथ ही यह जोख़िम भी थोड़ा कम हुआ जो ऐसी फ़िल्मों के सिंगल स्क्रीन पर रिलीज़ के समय होता था। पहले जिसे ‘आर्ट फ़िल्म टाइप’ कहा जाता था, वह भी अब एक नए ढंग से मल्टीप्लेक्स में दर्शक के सामने आने लगी थी। यह पूरी तरह कला फ़िल्म भी नहीं थी और व्यवसाय भी कर रही थी। इससे निश्चित रूप से कुछ नए विषयों पर फ़िल्में बनीं जिन्हें इससे पहले बनाना बहुत जोख़िम का काम था। ‘तारे ज़मीं पर’, ‘विकी डोनर’, ‘बर्फ़ी’, ‘न्यूटन’, ‘रॉक स्टार’, ‘दम लगाके हईशा’, ‘लंच बॉक्स’, ‘आर्टिकल 15’ जैसी फ़िल्में भी इस कारण भी चल पाईं क्योंकि इन्हें मल्टीप्लेक्स का दर्शक मिला। इनमें से कुछ औसत रहीं, कुछ हिट हुईं और कुछ सुपर हिट भी हो गईं। इन फ़िल्मों ने हीरो की परंपरागत छवि को तोड़ा और कुछ अलग कहने की कोशिश की। हिंदी सिनेमा का दर्शक भी अब कुछ नया देखना चाहता था।
लेकिन इस दौरान टीवी के ज़रिए दक्षिण की फ़िल्मों ने दर्शकों के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखी। ‘गोल्डमाइंस टेलीफ़िल्म्स’ जैसी कम्पनियों की इसमें विशेष भूमिका रही जिसके पास दक्षिण की फ़िल्मों की डबिंग का काम भी था और यह निजी टीवी चैनलों को फ़िल्मों के सैटेलाइट अधिकार भी दिलाती थी। इन कंपनियों के ज़रिए दक्षिण की ढेरों फ़िल्में हिंदी में डब होकर दर्शकों तक पहुँचीं। डब की हुई फ़िल्मों के अधिकार खरीदना इन टीवी चैनलों को सस्ता पड़ता था और विज्ञापनों के ज़रिए ज़्यादा कमाई हो जाती थी। इसके उलट नई हिंदी फ़िल्मों के सैटेलाइट अधिकार महँगे होते थे। लिहाज़ा धीरे-धीरे इन टीवी चैनलों से हिंदी फ़िल्में गायब होती चली गईं और दक्षिण की डब की हुई फ़िल्मों की बाढ़ सी आ गई। इस तरह ‘हीरो’ की जो छवि मल्टीप्लेक्स में देखने को नहीं मिल रही थी, वह कहीं न कहीं हिंदी के दर्शक के लिए टीवी पर अब भी बची हुई थी। यह सब उस वक्त शुरू हो चुका था जब आम दर्शक के लिए इंटरनेट के दरवाज़े नहीं खुले थे। इन टीवी चैनलों ने हिंदी दर्शक और दक्षिण की फ़िल्मों के बीच की दूरी को पाटने का काम किया। जो दर्शक इन फ़िल्मों के ‘फ़ैन’ नहीं थे, वे भी कम से कम इन फ़िल्मों के नायक-नायिकाओं को जानने लगे। रजनीकांत, कमल हासन, नागार्जुन, चिरंजीवी, अरविंदम स्वामी, प्रभु देवा, जैसे कलाकारों को तो हिंदी का दर्शक पहले से जानता था, लेकिन अब अल्लू अर्जुन, प्रभास, विजय सेतुपति, कार्थी, राना दग्गुबती, अनुष्का शेट्टी जैसे कई नए सितारे भी टीवी के ज़रिए हिंदी के दर्शक से जुड़ने लगे। कम से कम इनके चेहरे तो जाने-पहचाने हो ही गए। काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, तमन्ना भाटिया जैसी अभिनेत्रियों ने दक्षिण में किस्मत आज़माई और कामयाब रहीं। इस बीच आर माधवन, प्रकाश राज, तापसी पन्नू, जेनेलिया डिसूज़ा जैसे कलाकार दक्षिण के अलावा हिंदी फ़िल्मों में भी नज़र आते रहे। दक्षिण की इन फ़िल्मों की लोकप्रियता के चलते बॉलीवुड में धड़ल्ले से इनके रीमेक होने लगे। ‘हेरा फेरी’, ‘विरासत’ से लेकर ‘गजनी’, ‘सिंघम’, ‘दृश्यम’ जैसी रीमेक फ़िल्मों में अनिल कपूर, सलमान खान, शाहरुख़ खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बॉलीवुड के बड़े सितारों ने काम किया। ये फ़िल्में हिंदी में काफ़ी सफल भी रहीं। इनमें से कई फ़िल्मों में ड्रामा और एक्शन की भरपूर गुंजाइश थी। इनमें नायक एक कॉमिक हीरो की तरह वापस लौटा जो हिंदी फ़िल्मों से एक तरह से गायब हो चुका था। इन फ़िल्मों ने सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स, दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया।
इंटरनेट युग, यू ट्यूब और ओटीटी
पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का हर जगह विस्तार हुआ। गाँवों तक में, जहाँ कुछ समय पहले तक दूरदर्शन के अलावा कम ही चैनल पहुँच पाते थे, अब यूट्यूब पहुँच चुका था। जिस पर मनोरंजन के लिए काफ़ी कुछ मौजूद था। युवा पीढ़ी के लिए यह मनोरंजन का नया साधन बन गया जहाँ एक-डेढ़ जीबी प्रतिदिन के नेट पैक के साथ रोज़ फ़िल्में देखी जा सकती थीं या डाउनलोड की जा सकती थीं। यहाँ भी ‘गोल्डमाइंस’ जैसे यूट्यूब चैनलों के ज़रिए दक्षिण की फ़िल्में भारी तादाद में उपलब्ध कराई गईं और देखी भी गईं। कोविड महामारी के दौरान स्थितियाँ और तेज़ी से बदलीं। फ़िल्मों को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया जा सकता था इसलिए सीधे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ किया जाने लगा। दो सालों के लॉकडाउन के दौरान एमेज़ॉन, नेटफ़्लिक्स जैसे कई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़े। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ़ 2020 में ही भारत में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के सब्सक्राइबर्स की संख्या 60% तक बढ़ चुकी थी। इस सबका एक असर यह हुआ कि नई फ़िल्में घर बैठे देखने को मिलने लगीं। लॉकडाउन के बाद यह चलन और तेज़ी से बढ़ गया कि फ़िल्मों को सिनेमा हॉल से उतरने के बाद सीधे किसी न किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ किया जाने लगा। इससे फ़िल्मों की कमाई का एक और रास्ता तो खुला ही, दर्शक को भी ताज़ा फ़िल्में देखने का मौका मिलने लगा। हालाँकि, पायरेसी की समस्या पहले से ज़्यादा बढ़ गई।
कुल मिलाकर अब लोगों के पास कई तरह का कंटेंट आने लगा। इसमें हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती; हर भाषा का कंटेंट था। अंग्रेज़ी फ़िल्में और वेब सीरीज़ तो थी हीं। अब कोई भी नई सीरीज़ आते ही उसे रात भर में देख डालने (बिंज वॉच) का चलन शुरू हो गया। ओटीटी पर अब दुनिया भर का कंटेंट उपलब्ध था। दर्शक अब ‘पंचायत’ से लेकर ‘गेम ऑफ़ थ्रोन्स’ तक, जो चाहे देख सकते थे। ओटीटी अपने खुद के ओरिजिनल शो बना ही रहा था। भाषा के ‘लोकलाइज़ेशन’ ने इसमें काफ़ी मदद की। ज़्यादातर कंटेंट या तो हिंदी डबिंग या हिंदी सबटाइटल्स के साथ उपलब्ध होने लगा। इससे हुआ यह कि कई अच्छी फ़िल्में और सीरीज़ अपने मूल रूप में देखने को मिलने लगीं और उनके रीमेक की ज़रूरत ख़त्म होने लगी। अंग्रेज़ी के अलावा आज कई स्पेनिश और कोरियाई शो भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं।
ओटीटी और यूट्यूब के दर्शक के पास अब पूरी दुनिया का मनोरंजन कंटेंट है। वह विदेशी कंटेंट के साथ-साथ दक्षिण का भी काफ़ी कुछ कंटेंट अपने मूल रूप में देख चुका है। अब वह सिनेमाहॉल में अच्छे कंटेंट की तलाश में आता है, भले ही वह कहानी के स्तर पर मिले या फिर तकनीक के स्तर पर। आज दक्षिण के निर्देशक भव्य और अच्छी तकनीक वाली फ़िल्में बना रहे हैं। इनकी कहानी भी दिलचस्प होती है और विज़ुअल इफ़ेक्ट्स भी। राजामौली की फ़िल्म ‘आरआरआर’ की सिनेमेटोग्राफ़ी को पूरे भारत के अलावा विदेशों में भी सराहा गया। दक्षिण के राज्यों में फ़िल्मों की बम्पर कमाई का एक बड़ा कारण यह भी बनता है कि वहाँ स्क्रीनों की संख्या बाकी भारत से काफ़ी ज़्यादा (पूरे देश का लगभग 50%) है। फ़िल्म देखते ही देखते ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ‘विक्रम’ और ‘पीएस-1, 2’ ने उत्तर और मध्य भारत में दक्षिण के मुकाबले बहुत कम कमाई की, लेकिन देश भर और दुनिया भर में बेहद सफल साबित हुईं। पहले हॉलीवुड की ‘पाइरेट्स ऑफ़ कैरेबियन’ जैसी फ़िल्मों के बारे में सुनने को मिलता था कि फ़िल्म का सीक्वल भी साथ में फ़िल्मा लिया गया है। पिछले कुछ सालों में यह हमारे यहाँ भी देखने को मिलने लगा है। मणिरत्नम की ‘पीएस-1’ और अयान मुखर्जी की ‘ब्रह्मास्त्र’ में यही किया गया। एक समय था जब फ़िल्म के सीक्वल कम ही सफल रहते थे। लेकिन ‘बाहुबली-2’ और ‘केजीएफ़-2’ जैसी फ़िल्मों ने साबित कर दिया कि भारत में भी सीक्वल-प्रीक्वल ताबड़तोड़ कमाई कर सकते हैं।
हॉलीवुड के मार्वल स्टूडियो की फ़िल्मों ने दुनिया भर में अपार लोकप्रियता हासिल की है। इन्होंने हमारे यहाँ की फ़िल्मों पर भी गहरा असर डाला है। बॉलीवुड फ़िल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में भी मार्वल की तर्ज पर ‘अस्त्रवर्स’ रचने की कोशिश की गई। इसमें ‘एवेंजर्स’ की तरह कई सारे सुपर हीरो खड़े करने की कोशिश थी और ‘स्टोन्स’ की जगह ब्रह्मास्त्र के तीन टुकड़े थे जिन्हें पा लेना यानी सर्वशक्तिमान हो जाना था, बिल्कुल थेनॉस की तरह! थोड़ी बहुत ‘इंस्पिरेशन’ और कमज़ोर स्क्रीन प्ले के बावजूद फ़िल्म चल गई। कम से कम फ़िल्म के विज़ुअल इफ़ेक्ट वाले पक्ष पर अच्छा काम किया गया था। दूसरी तरफ़ टी-सीरीज़ की फ़िल्म ‘आदिपुरुष’ को ख़राब वीएफ़एक्स के चलते भयानक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
‘साउथ’ की फ़िल्म इंडस्ट्री
दक्षिण के सिनेमा में नायक की ‘लार्जर दैन लाइफ़’ छवि को फिर से बनाने का काम किया, दूसरी तरफ़ वहाँ के अभिनेताओं की सहजता भी लोगों को भा रही है। विजय सेतुपति, फ़हाद फ़ाज़िल जैसे अभिनेता देश भर में पहचान बना चुके हैं। ये लोग बिना सिक्स पैक ऐब्स के, अपने अभिनय के दम पर टिके हुए हैं। ऐसा नहीं कि दक्षिण में सिर्फ़ ‘मास’ फ़िल्में ही बन रही हैं या कारोबार कर रही हैं। कई संवेदनशील और अलग विषयों पर वहाँ पहले भी फ़िल्में बनती रही हैं। ‘केजीएफ़’ ने कन्नड़ इंडस्ट्री को प्राणवायु देने का काम किया। इस तरह की मास फ़िल्म के अलावा वहाँ पिछले दिनों आईं फ़िल्मों ‘गरुड़ा गमना वृषभ वाहना’ और ‘777 चार्ली’ को अपने अलग कंटेंट और स्क्रीनप्ले की वजह से हर तरफ़ प्रशंसा मिली। ‘कांतारा’ सिर्फ़ 16 करोड़ की लागत से बनी लेकिन दिलचस्प कहानी और उम्दा सिनेमैटोग्राफ़ी के कारण हालत यह हुई कि दर्शकों की माँग पर उसे हिंदी में भी रिलीज़ किया गया। मलयालम इंडस्ट्री में इन दिनों जैसे फ़िल्मों की बाढ़ आई हुई है। वहाँ पिछले कुछ सालों में कई तरह की फ़िल्में बनीं। ‘दृश्यम 1 और 2’ जैसी थ्रिलर फ़िल्में बनी, वहीं ‘जल्लिकट्टू’ और ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ जैसी विचारपरक फ़िल्में भी बनीं, केरल की बाढ़ आपदा पर ‘2018’ बनी। हाल ही में ‘प्रेमलु’, ‘भ्रमयुगम’, ‘आडुजीविथम’ और ‘मंजुमेल बॉयज़’, ‘रोमांचम’ जैसी फ़िल्में भी बहुत चर्चित हुईं।
तमिल में ‘कैथी’, ‘विक्रम’, ‘विक्रम वेधा’, ‘जेलर’ जैसी सफल एक्शन थ्रिलर फ़िल्में तो बनी हीं, साथ ही ‘जय भीम’ जैसी विचारोत्तेजक और’पीएस 1,2′ इतिहास-आधारित और हाल ही में आई ‘महाराजा’ जैसी थ्रिलर फ़िल्म भी बनी। कल्कि के उपन्यास ‘पोनियिन सेल्वन’ पर आधारित ‘पीएस-1’ ने पहली बार बड़े परदे पर दक्षिण के किसी राजवंश को भव्यता और गंभीरता से दिखाया। तेलुगु में ‘बाहुबली’, ‘आरआरआर’, ‘पुष्पा’, ‘सालार’ के अलावा ‘सीता रामम’ और ‘हाए नन्ना’ जैसी फ़िल्में भी बनी हैं।
सबका सिनेमा
हिंदी बेल्ट में दक्षिण की फ़िल्मों की ‘साउथ की पिक्चर’ वाली छवि अब काफ़ी बदल चुकी है। यहाँ इनकी स्वीकृति और माँग दोनों बढ़ी हैं। कलाकारों को दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। पैन इंडिया स्तर पर प्रदर्शन के कारण अब फ़िल्मों में दक्षिण और बॉलीवुड के कलाकार मिलकर काम कर रहे हैं। ‘रॉकेटरी’ में शाहरुख़ खान आए, ‘आरआरआर’ में अजय देवगन और आलिया भट्ट अहम भूमिकाओं में नज़र आए, ‘पीएस-1,2’ में ऐश्वर्या राय एक तरह से मुख्य भूमिका में थीं। ‘कल्कि’ और ‘मैरी क्रिसमस’ जैसी फ़िल्मों में भी यही देखने को मिला। अब भारत में बनने वाली कई फ़िल्में पूरे देश की फ़िल्म के रूप में सामने आ रही हैं। कई अभिनेता कह भी रहे हैं कि अब ‘बॉलीवुड’, ‘टॉलीवुड’, ‘कॉलीवुड’ वगैरह कहना बंद करके भारत में कहीं भी बनने वाली फ़िल्म को पूरे देश की फ़िल्म माना जाना चाहिए।
दक्षिण की फ़िल्मों को हिंदी के दर्शक तक पहुँचाने में डबिंग इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका रही है। पहले की बनिस्बत आज डबिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले की फ़िल्मों में हिंदी डबिंग का स्तर इतना अच्छा नहीं होता था। संकेत म्हात्रे, जो हॉलीवुड की फ़िल्मों के अलावा दक्षिण भारत की फ़िल्मों के हिंदी डब में सूर्या, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू जैसे अभिनेताओं को आवाज़ दे चुके हैं, ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ साल पहले तक डबिंग स्क्रिप्ट में कई तरह की गलतियाँ हुआ करती थीं जिन्हें सुधारने की ज़िम्मेदारी डबिंग डायरेक्टर और वॉइस एक्टर की होती थी। लेकिन आज वॉइस एक्टर को यह बहुत अच्छे स्वरूप में मिलने लगी है। नतीजतन अब हिंदी में डब की हुई फ़िल्मों की भाषा भी काफ़ी हद तक मूल हिंदी फ़िल्म जैसी लगती है। कोविड के पहले यूट्यूब पर फ़िल्म रिव्यू के चैनल बहुत कम थे। ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही थे। लेकिन पिछले तीन-चार सालों में जिस तरह से हिंदी समेत अलग-अलग भाषाओं के फ़िल्म रिव्यू चैनलों में इज़ाफ़ा हुआ है, उससे दर्शक को कम से कम फ़िल्म की मोटी जानकारी तो मिल ही जाती है। ये चैनल भी बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में देश भर की फ़िल्मों की जानकारी आम दर्शक तक पहुँचा देते हैं। कुछ समय पहले आई उड़िया फ़िल्म ‘दमन’ के बारे में भी इन्हीं चैनलों के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चला जिसे बाद में हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था।
ऐसे समय में अब फ़िल्मों को उनके मूल रूप में देखकर भी आनंद लिया जा सकता है। अब भारत में बनने वाली हर अच्छी फ़िल्म को ‘भारतीय फ़िल्म’ की तरह देखा और सराहा जाने लगा है। रीमेक यकीनन रचनात्मकता और चुनौती भरा काम है। ‘दृश्यम’ जैसी इक्का-दुक्का फ़िल्मों को छोड़ दें तो हाल ही में हिंदी सिनेमा की ज़्यादातर रीमेक फ़िल्में कुछ खास नहीं कर पाईं। तमिल फ़िल्म ‘विक्रम वेधा’ के हिंदी रीमेक में ऋतिक रोशन के अभिनय की बहुत तारीफ़ हुई। लेकिन वही कहानी दिखाने में नएपन की कितनी गुंजाइश निकल पाई? कम बजट होने के कारण जहाँ मूल फ़िल्म ने अपने बजट से लगभग 5 गुना कमाई की थी वहीं इसकी हिंदी रीमेक का बजट भारी-भरकम होने का कारण यह अपनी लागत भी नहीं निकाल सकी। अजय देवगन की ‘भोला’ भी कार्थी की ‘कैथी’ जैसा प्रभाव पैदा नहीं कर पाई। यही हाल अक्षय कुमार की ‘कटपुतली’, ‘सरफिरा’ और कार्तिक आर्यन की ‘शहज़ादा’ का भी रहा। हॉलीवुड फ़िल्म का रीमेक बनाना अब ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। बाधा अब तकनीक का अभाव नहीं है बल्कि ‘ओरिजिनल’ का सुलभ हो जाना है। कुछ समय पहले आई हॉलीवुड की रीमेक फ़िल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में आमिर खान ने ‘फ़ॉरेस्ट गंप’ की मूल भावना को पकड़ने की कोशिश तो की लेकिन कई जगह वे चूक गए। फ़िल्म को भारतीय संदर्भ में देखते हुए उसमें कई रचनात्मक बदलाव ज़रूर किए गए लेकिन इन्होंने फ़िल्म को बेहतर बनाने के बजाय कहानी का मज़ा ख़राब ही किया। जो गहराई मूल फ़िल्म में थी, वह रीमेक में महसूस नहीं हुई। फ़िल्म में आमिर पर अपनी ही पुरानी भूमिकाओं की झलक दिखाई दी। आमिर पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह की फ़िल्में बना चुके हैं, दर्शक उनसे अब ज़्यादा रचनात्मक होने की उम्मीद करते हैं।
इसी बीच हिंदी में कई मौलिक फ़िल्में आईं जिनमें से कई ने अच्छी कमाई की और कई ने अच्छा कंटेंट भी दिया। 2023 का साल शाहरुख़ के नाम रहा जिनकी ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’, तीनों फ़िल्में हिट रहीं। ‘पठान’ आदित्य चोपड़ा की एक एक्शन फ़िल्म थी। एटली की ‘जवान’ ने अपने ‘मास सिनेमा के फ़्लेवर’ को बनाए रखते हुए कई सामाजिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की। ‘डंकी’ में राजकुमार हिरानी ने भारत से अवैध रूप से विदेश जाने वाले लोगों और उनकी समस्याओं को केंद्र में रखा। ‘गंगुबाई काठियावाड़ी’, ‘भूल भुलैया-2’, ‘द कश्मीर फ़ाइल्स’, ‘ओह माय गॉड-2’ और ‘एनिमल’ जैसी फ़िल्मों ने बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छी कमाई की, वहीं ‘चुप’, ‘कला’, ‘ट्वेल्थ फ़ेल’, ‘बवाल’, ‘कटहल’, ‘पिप्पा’, ‘लव ऑल’, ‘जोरम’, ‘आर्टिकल 370’, ‘अमरसिंह चमकीला’, ‘लापता लेडीज़’, ‘श्रीकांत’ जैसी फ़िल्मों को उनके कंटेंट या स्क्रीन प्ले के कारण पसंद किया गया। करण जौहर और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित और निखिल नागेश भट निर्देशित हाल ही में आई फ़िल्म ‘किल’ को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी पसंद किया गया। पहली बार यह सुनने को मिला कि कोई हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस किसी भारतीय फ़िल्म का रीमेक बनाने जा रहा है। बॉलीवुड के लिए यह वाकई एक अच्छी खबर है।
आज के दौर में भारत में कुशल तकनीशियनों की कमी नहीं है। विदेशों से भी तकनीकी मदद लेना अब बहुत आसान हो गया है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स में हम हॉलीवुड के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। लेकिन बदलते हुए दौर में भारतीय सिनेमा को अपनी मौलिकता पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हर फ़िल्म में ज़बरदस्ती गाने या एक्शन ठूँसना और प्रेम कहानियों का दोहराव करना अब पुरानी बात हो गई है। कई फ़िल्में में यह साबित हो चुका है कि इस सबके बिना भी फ़िल्में चलती हैं और पसंद की जाती हैं। भारतीय दर्शक का नज़रिया अब व्यापक हो रहा है। अब ज़रूरत है कि रीमेक या बेवजह के धूम-धड़ाके के बजाय मौलिकता और नवीनता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
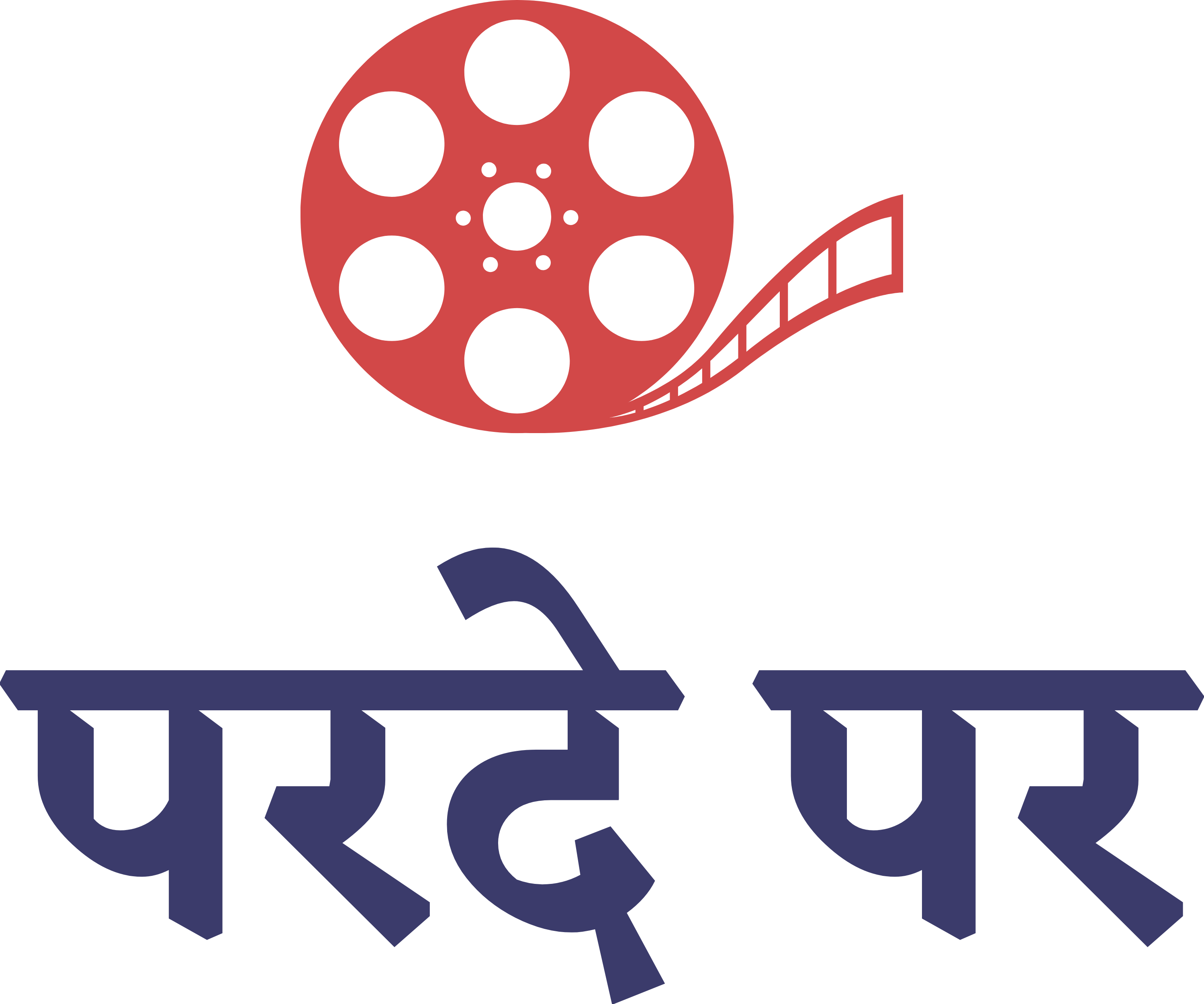
शानदार आलेख बंधु,
बदलती टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से नई पीढ़ी की सोच पर व्यापक असर डाला है,ठीक उसी तरह मनोरंजन के इस क्षेत्र में भी आमूलचूल बदलाव देखने को मिले है। पहले के समय में फ़िल्म देखने पूरे परिवार के साथ थियेटर में जाना किसी उत्सव से कम नहीं था वहीं आज सभी लोग अपने बचे हुए समय में कभी भी ओटीटी पर सिनेमा, वेब सीरीज,सीरियल से लेकर खेल तक भी देख सकते है। जिस तरह से नया कंटेंट आज की फिल्मों और वेब सीरीज में देखने को मिल रहा है ये कहीं न कहीं नई पीढ़ी की सोच का असर है,जो पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिल रहा है। वरना पिछले कुछ दशकों में वही घिसी पीटी प्रेम कहानी और फूहड़ कॉमेडी, फिल्मों का पर्याय बन चुकी थी।
अब देखना होगा कि आने वाले समय में कहानी और तकनीक का यह मिश्रण हमें किन ऊंचाइयों तक ले कर जाएगा। क्योंकि तकनीक ने विश्व सिनेमा तक हमारी पहुंच तो बढ़ा दी है लेकिन कहीं न कहीं अभी भी हमारा सिनेमा, विश्व के उस सिनेमा से पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। हिंदी लघु फिल्मों और मराठी सिनेमा ने संवेदनशील विषयों को लेकर कुछ हद तक अपनी पहुंच बढ़ाई है। इस फिल्मों का मेन स्ट्रीम सिनेमा में आना अभी भी बाकी है।
लेख के लिए बहुत बहुत बधाई दादा💐। फिल्मों पर लगभग सभी तरह के दृष्टिकोण को अपने में समेटता आलेख।
इस विस्तृत टिप्पणी के लिए बहुत शुक्रिया भाई!
सही कहा, कहानी और तकनीक का सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है.