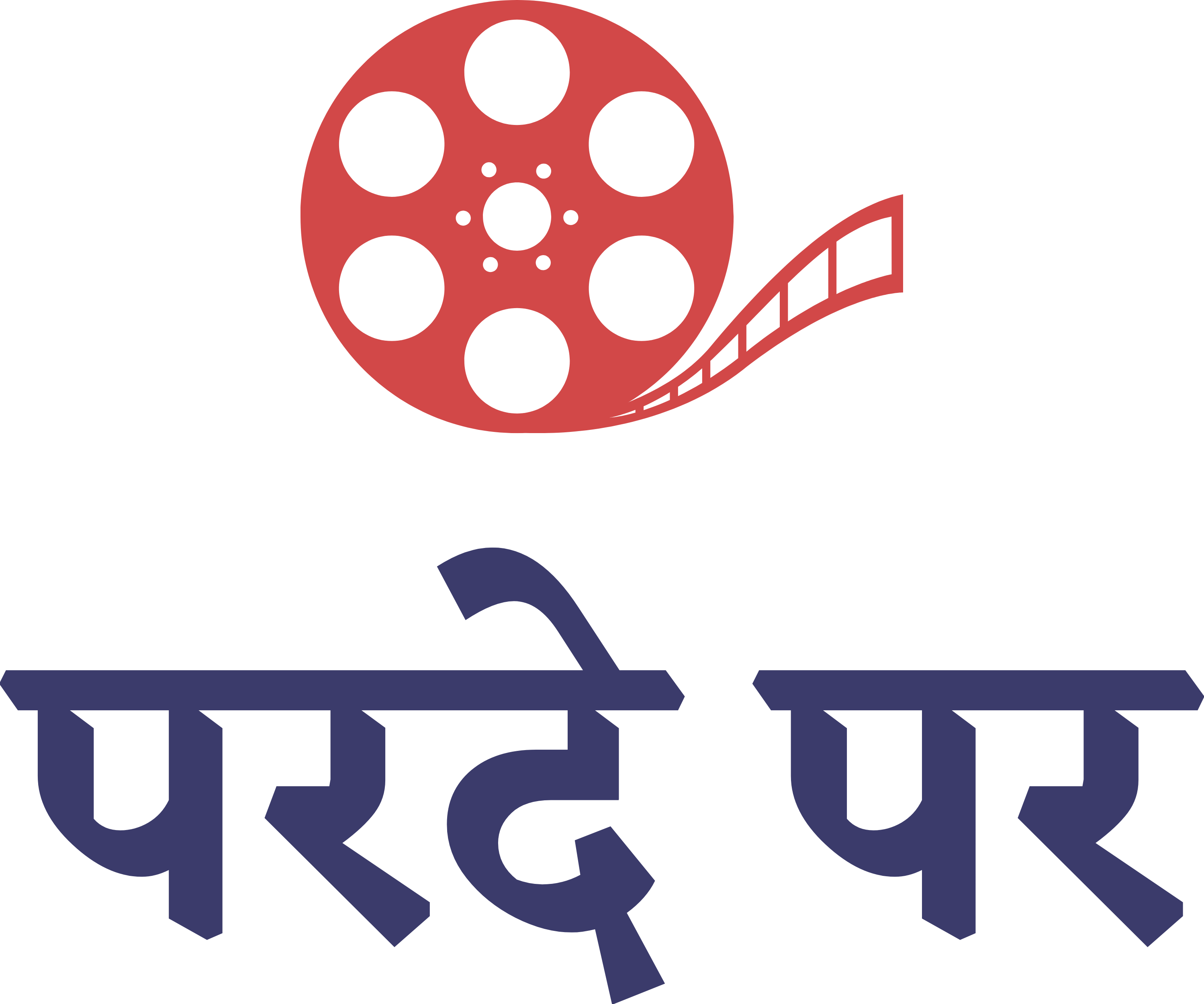आज फ़िल्मों को हम जिस रूप में देखते हैं उसके पीछे सिनेमा ने एक लंबा सफ़र तय किया है. अब फ़िल्में बड़े-बड़े आईमैक्स कैमरों से शूट हो रही हैं और वैसी ही भव्य स्क्रीनों पर दिखाई जा रही हैं. वीएफ़एक्स ने फ़िल्म देखने के हमारे अनुभव को एक अलग ही स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है. इंटरनेट और फिर ओटीटी के आने के बाद अब दर्शक की सिनेमा को देखने की दृष्टि और व्यापक हो गई है. फ़िल्में बनते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँच सकती हैं. किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पर हर रोज़ नया कंटेंट आ रहा है. लेकिन सिनेमा को यहाँ तक पहुँचाने में हरेक तकनीक, हरेक प्रयोग का अपना महत्त्व रहा है.
‘पश्चिम और सिनेमा’ (Pashchim Aur Cinema) हिंदी में लिखी उन किताबों में से है जो विश्व सिनेमा की समझ बनाने में बहुत मदद करती है. इस किताब के लेखक दिनेश श्रीनेत (Dinesh Shrinet) हैं जो एक लंबे समय से सिनेमा को लेकर बहुत गंभीर ढंग से लिखते रहे हैं. किताब का पहला संस्करण साल 2012 में ‘वाणी प्रकाशन’ से आया था. इसमें सिनेमा की इस यात्रा को कई अहम फ़िल्मों का ज़िक्र करते हुए दिखाया गया है. बीच-बीच में फ़िल्मों के कई स्क्रीनशॉट और पोस्टर भी शामिल किए गए हैं जो कई चीज़ों से सीधे कनेक्ट होने में हमारी मदद करते हैं.
लेखक ने इस पूरी किताब को चार हिस्सों में बाँटा है – 1. परछाइयों का देश, 2. इतिहास से मुठभेड़, 3. फ़िल्म जॉनर और 4. पश्चिम से पूरब की ओर. किताब की शुरुआत में लेखक सिनेमा के उद्गम की बात करते हैं. वे 1895 के उस ऐतिहासिक पल से शुरुआत करते हैं जब पेरिस में लुमिएर ब्रदर्स ने दुनिया की पहली फ़िल्म का प्रदर्शन किया था. हम उस रोमांच की सिर्फ़ कल्पना ही कर सकते हैं जो उस समय लोगों ने पहली बार परदे पर गतिमान छवियों को देखते हुए महसूस किया होगा. लेखक यहाँ उस समय लुमिएर ब्रदर्स और टॉमस अल्वा एडिसन के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के बारे में भी बताते हैं. फिर हम देखते हैं कि किस तरह फ़िल्मों के विकास में नए पहलू जुड़ते चले गए. यहाँ ‘द ग्रेट ट्रेन रॉबरी’ से लेकर ‘ए ट्रिप टू द मून’ और ‘बैटलशिप पोटेम्किन’ जैसी कई महत्त्वपूर्ण फ़िल्मों का उल्लेख किया गया है. हमें पता चलता है कि पुडोवकिन और आइजेंस्ताइन ने किस तरह ‘मोंताज’ तकनीक का विकास किया जो आज भी सिनेमा का एक अहम हिस्सा है. इसी तरह स्लो मोशन और रिवर्स जैसी कई तकनीकों पर पर भी विस्तार से बात की गई है. यह किताब हमें बताती है रूसी सिनेमा का विश्व सिनेमा में क्या योगदान रहा. लेखक आगे इटली के नवयथार्थवाद (नियोरियलिज़्म) की बात करते हैं. यहाँ ‘बाइसिकल थीव्स’ जैसी फ़िल्मों का उल्लेख मिलता है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया के सिनेमा पर गहरा असर डाला. फ़्रांस के सिनेमा की बात करते हुए बताया गया है कि किस तरह वहाँ गोदार, त्रुफो जैसे फ़िल्मकारों ने ऑतर (या ऑथर) थियरी को विकसित किया. लेखक इसके बाद जर्मन अभिव्यंजनावाद (एक्सप्रेशनिज़्म) की बात करते हैं और अल्फ़्रेड हिचकॉक पर इसका किस तरह असर पड़ा.
किताब में आगे हमें हॉलीवुड की कई क्लासिक फ़िल्मों का उल्लेख भी मिलता है जैसे – ‘कासाब्लांका’, ‘इट हैप्पन्ड वन नाइट’, ‘सिटिज़न केन’, ‘सिटी लाइट्स’ आदि. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टेलीविजन के आने के बाद सिनेमा पर किस तरह असर पड़ा. आगे के लेखों में थर्ड सिनेमा और कई आंदोलनों पर बात की गई है, सिनेमा के अलग-अलग जॉनर के बारे में बात की गई है जैसे यूरोप का आर्ट सिनेमा, वेस्टर्न सिनेमा, फ़िल्म नॉयर, अपराध फ़िल्में, थ्रिलर, डायस्टोपियन सिनेमा, मॉन्स्टर फ़िल्में, युद्ध फ़िल्में आदि. लेखक ने इन फ़िल्मों की शुरुआत से लेकर आज बन रहीं उस जॉनर की फ़िल्मों पर बात की है. हालाँकि बाद के ये लेख इन्फ़र्मेटिव ज़्यादा हैं इसलिए पढ़ते हुए रोचकता में थोड़ी सी कमी महसूस होती है. आखिरी खंड में लेखक ने भारतीय सिनेमा के अलग-अलग जॉनर पर बात की है जो किसी न किसी तरह विश्व सिनेमा से प्रभावित रहे. यह किताब चूँकि साल 2012 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इसमें उस समय तक की फ़िल्मों का उल्लेख ही मिलता है लेकिन सिनेमा के आज तक के सफ़र को समझने के लिए यह काफ़ी है.
यह किताब हमें विश्व सिनेमा के कई महत्वपूर्ण पड़ावों से रूबरू करवाती है. सिनेमा के हर पड़ाव को एक किताब में समेटना बहुत मुश्किल काम है, निश्चित रूप से कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी. लेकिन इस सबके बावजूद यह किताब सिनेमा पर बहुत रोचक ढंग से प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवाती है. साथ ही यह फ़िल्मों को देखने के हमारे नज़रिए को परिष्कृत करने में भी काफ़ी मदद करती है.