मीडिया की भूमिका और इसके दायित्व को लेकर हमारे यहाँ अलग-अलग तरह से फ़िल्में बनी हैं। साल 1989 में टीनू आनन्द के निर्देशन में एक फ़िल्म बनी थी – ‘मैं आज़ाद हूँ’। उस समय हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर दूरदर्शन ही था जिसका काम सिर्फ़ समाचार देने तक सीमित था। पत्रकारिता का सारा दारोमदार प्रिंट मीडिया पर ही था। अमिताभ बच्चन और शबाना आज़मी अभिनीत इस फ़िल्म में बताया गया था कि किस तरह एक अखबार खबरों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक काल्पनिक चरित्र को गढ़ता है और फिर उसे एक असल इंसान से जोड़ दिया जाता है। साल 2000 में शाहरुख, जूही चावला, परेश रावल की एक फ़िल्म आई – ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’। इसमें न्यूज़ चैनलों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और टीआरपी की भूख को लेकर बहुत तीखा व्यंग्य था। हालाँकि यह फ़िल्म खास सफल नहीं हो पाई। उसी दौर में एक और फ़िल्म आई – ‘नायक’। अनिल कपूर, परेश रावल और अमरीश पुरी ने इसमें यादगार भूमिकाएँ निभाईं। थोड़ी नाटकीयता के बावजूद इस फ़िल्म ने मज़बूती से यह संदेश दिया कि सीधा सवाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। साल 2010 में आई अनूशा रिज़वी की फ़िल्म ‘पीपली लाइव’ ने एक साथ दो मुद्दों को उठाया। एक तरफ़ इसमें किसानों की आत्महत्या और मुआवज़े पर बहस थी वहीं सनसनी ढूँढने निकले मीडिया पर करारा व्यंग्य भी था। रघुवीर यादव के गाए ‘महंगाई डायन…’ को कौन भूल सकता है! राम माधवानी निर्देशित कार्तिक आर्यन की कुछ ही समय पहले आई फ़िल्म ‘धमाका’ (2021) भी टीआरपी की इसी होड़ पर आधारित थी। मीडिया में पैसा लेकर खबरों को दबाने, ईमानदार पत्रकारों की मेहनत से बनाई हुई स्टोरी को चोरी करके अवॉर्ड हासिल करने जैसे मुद्दों को इसने प्रभावी ढंग से उठाया।
इंटरनेट के प्रसार के बाद अब मीडिया का एक नया डाइमेंशन खुल गया है जो धीरे-धीरे मेनस्ट्रीम मीडिया के मज़बूत विकल्प की तरह सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के साथ यह तेज़ी से लोगों के बीच अपनी अप्रोच बढ़ा भी रहा है। यू ट्यूब पर कई न्यूज़ चैनल बन गए हैं। यहाँ विश्वसनीयता निश्चित रूप से बहस का विषय हो सकती है लेकिन कई चैनल लगातार अच्छा और गम्भीर कंटेंट देकर सार्थक बहस के लिए और जगह बना रहे हैं।
हाल ही में नेटफ़्लिक्स (Netflix) पर रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘भक्षक’ (Bhakshak) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बन रहे इसी नए रास्ते को उम्मीद की तरह देखती है। यह फ़िल्म मुज़फ़्फ़रपुर में 2018 में अनाथ लड़कियों के एक शेल्टर होम में उनके साथ हो रहे यौन शोषण के एक सच्चे वाकए से प्रेरित बताई जाती है जिसमें एक पत्रकार के साहस ने ऐसे सच को उजागर किया था जिसे देखकर भी अनदेखा किया जा रहा था। चूँकि आज भी एक बड़ा तबका मेनस्ट्रीम मीडिया को ही देखता-सुनता है, खबरों का बड़े पैमाने पर प्रसार इसी मीडिया के ज़रिए होता है। अपराधी कई बार इतना ताकतवर होता है कि उसके गिरहबान तक कानून के हाथ भी नहीं पहुँच पाते। सत्ता के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव के चलते इस तरह की कई ज़रूरी और चिंताजनक खबरें मेनस्ट्रीम मीडिया पर आती ही नहीं और एक सीमित दायरे में दम तोड़ देती हैं। यह फ़िल्म कई ज़रूरी मुद्दों को लेकर मीडिया की इस ‘चुप्पी’ पर भी सवालिया निशान लगाती है। यहीं सोशल मीडिया की भूमिका और ज़्यादा अहम हो जाती है। अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह की लड़ाइयों के लिए यह एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है और कई बार यह हुआ भी है।
फ़िल्म में भूमि पेडणेकर, संजय मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में हैं। संजय मिश्रा मंजे हुए कलाकार हैं और भारी-भरकम बजट वाली फ़िल्मों से लेकर छोटे बजट की ढेरों फ़िल्मों में कई तरह की भूमिकाएँ कर चुके हैं। भूमि ‘दम लगा के हईशा’, ‘सांड की आँख’, ‘टॉयलेट-एक प्रेम कथा’ जैसी फ़िल्मों के ज़रिए अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। लेकिन आदित्य श्रीवास्तव को फ़िल्म में देखने पर एहसास होता है कि ‘सीआईडी’ उनके करियर का लंबा समय खा गया। ‘बैंडिट क्वीन’ के बाद वे ‘सत्या’, ‘गुलाल’, ‘सुपर 30’ जैसी फ़िल्मों में आए लेकिन उनकी प्रतिभा का उस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा होना था। इस फ़िल्म में उनकी निगेटिव भूमिका असरदार है। ‘पंचायत’ के ‘बनराकस’ दुर्गेश कुमार और एसएसपी बनीं सई ताम्हणकर की भूमिकाएँ छोटीं लेकिन अहम हैं। शेल्टर होम को फ़िल्म में जिस तरह दिखाया गया है वह अनाथ लड़कियों की अंधेरे और नाउम्मीदी से भरी ज़िंदगी के क्रूर यथार्थ को हमारे सामने ला खड़ा करता है। फ़िल्म के कमज़ोर पक्ष भी हैं। कैमरामैन और खबर देने वाले के बीच संवादों में हास्य पैदा करने की कोशिश की गई है लेकिन वह बस ठीक ही लगी है। महिला पत्रकार का पति अपने भाई के बुरी तरह पिटने पर दुखी तो है लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी और तनाव दिखाई ही नहीं देता। छोटे से न्यूज़ चैनल ‘कोशिश टीवी’ के कुल जमा दो लोगों की टीम का इतनी उठापटक कर लेना कहीं-कहीं थोड़ा अधिक दुस्साहस भरा लगता है।
लेकिन इस सबके बावजूद निर्देशक पुलकित ने फ़िल्म की सहजता को कहीं खोने नहीं दिया है। उन्होंने भूमि को हीरो बनाकर कहानी पर हावी नहीं होने दिया और आखिर में उनके मोनोलॉग को उपदेश होने से भी बचाया है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों को अचानक ‘अभियान’ बनते दिखाने के क्लीशे से भी वे बचे हैं। फ़िल्म कई ऐसी जगहों पर खुद को रोक भी लेती है जहाँ से आगे जाने पर इसके बेहतर हो जाने या बिखर जाने, दोनों की संभावना थी। सच के लिए लड़ाई लड़ने वाले पत्रकारों को उनकी निजी ज़िंदगी और रिश्तों में जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे यह फ़िल्म अच्छी तरह दिखाती है। यह एक उम्मीद तो देती ही है लेकिन आखिर में बंसी साहू की मुस्कान के साथ कई सवाल भी छोड़ जाती है।
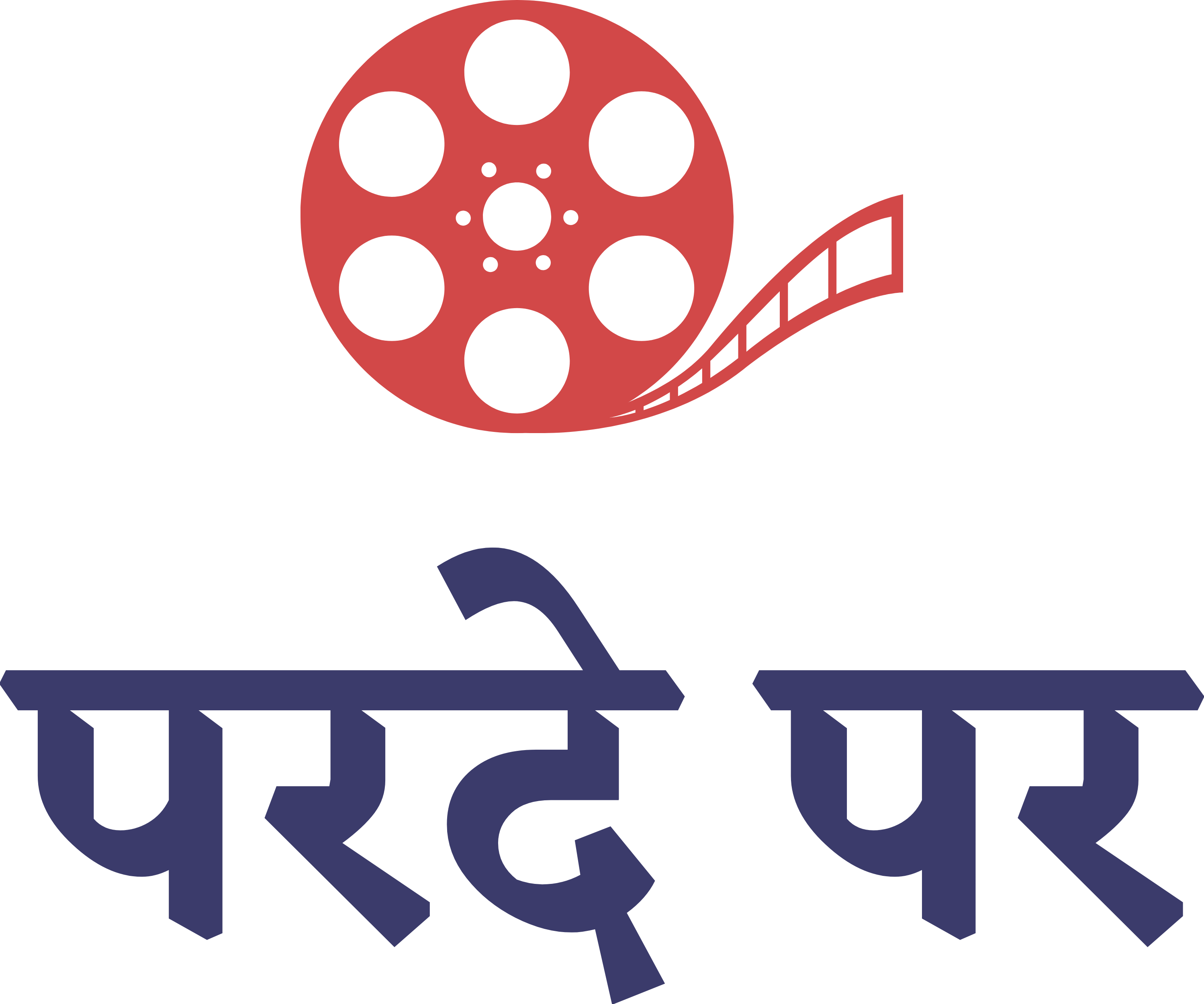
दिलचस्प !मीडिया की भूमिका के विषय पर फ़िल्मों की चर्चा से वाक़ई उन फ़िल्मों पर ध्यान गया !
इस फ़िल्म के प्रति उत्सुकता जागी है !
आपने समय निकालकर पढ़ा इसके लिए आभार!
Very well written👍🏻
Keep going🤝
Thank you so much!
अच्छा लिखा है। फ़िल्म देख ली है। फ़िल्म पर मेहनत कम हुई है। कई पक्ष बहुत ही कमज़ोर हैं। सच्ची घटनाओं पर फ़िल्म बना लेने से वह अच्छी हो जाएगी ऐसा नहीं है। फ़िल्म उस सच को जानने के लिए देखी जा सकती है।
सही कहा आपने। कई पक्षों पर और काम होना था। टिप्पणी के लिए बहुत आभार!
I agree. फ़िल्म कई ऐसी जगहों पर खुद को रोक भी लेती है जहाँ से आगे जाने पर इसके बेहतर हो जाने या बिखर जाने, दोनों की संभावना थी।
शुक्रिया भाई। समय निकालकर पढ़ा, इसके लिए भी।